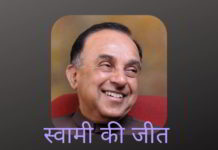कपित्था और जम्बू को भगवान गणेश का प्रसाद बनाया गया। उन्हें पीपल, बरगद और नीम के पेड़ों के नीचे घर दिया गया क्योंकि वे जल स्रोतों के उत्तम चिह्नक हैं।
क्या किसी ने सोचा है कि भगवान गणेश पर प्रसिद्ध श्लोक जो “गजाननं भूतगणादि सेवितं” (गजानन जिन्हें भूत गण आदि पूजते हैं) से शुरू होता है, अगली पंक्ति में ही सबसे पहले गणेश के भोजन के बारे में क्यों बात करता हैं? यह खाद्यपदार्थ आमतौर पर गणेश को चढ़ाया जाने वाला लोकप्रिय ‘मोदक‘ भी नहीं है। यह “कपित्थ जम्बू फलसरा” (कपित्थ जम्बूफल) – बेल और जामुन के फलों का मूल या सार है। ये दोनों फल विषम किस्म के हैं और बहुत मीठे भी नहीं होते। लेकिन अतीत में उनके बहुत से पेड़ पाए गए होंगे, यह इस तथ्य से पता चलता है कि हमारा देश ‘जम्बू-द्वेपा’ का हिस्सा है – जम्बू पेड़ों की विशाल भूमि। गणेश को इन दो फलों को प्रसाद के रूप में अर्पित करने के प्रारंभ की जांच में जल स्रोतों के ज्ञान को संरक्षित करने में हमारे ऋषियों के कुछ आश्चर्यजनक लेकिन सुविचारित तरीके सामने आते हैं, हां, आपने सही पढ़ा, जल स्रोत।
इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने लोगों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए पूजा के तरीके विकसित किए थे। आज सारस्वत द्वारा उल्लिखित कोई भी वृक्ष बहुतायत में नहीं पाए जाते हैं और इन वृक्षों के विनाश के कारण अब कोई जलमार्ग पहचाना नहीं जा सकता है।
गणेश और जल स्रोतों का अंतरंग संबंध है। वर्तमान पीढ़ी केवल गणेश उत्सव के अंत में मूर्तियों के विसर्जन समारोह के संदर्भ में ही पानी के बारे में सोच सकती है। लेकिन पुराने जमाने के लोगों को जलमार्गों के पास स्थापित गणेश की मूर्तियाँ याद होंगी। जहां कहीं भी जल निकाय होता, जैसे कोई तालाब या टैंक और वह चाहे कितना भी छोटा हो हम उस जल निकाय के पास एक पेड़ के नीचे गणेश रखे हुए देख सकते थे। अधिकांश स्थानों पर, वह जलमार्ग के पास स्वाभाविक रूप से बड़ा हुआ पीपल का पेड़ होता था। यह दक्षिण भारत में एक आम दृश्य था, जहां मंदिर की संस्कृति उत्तर भारत, जहां विदेशी आक्रमणों ने हजारों सालों से अधिकांश मंदिरों को मिटा दिया था, की तरह बर्बाद नहीं हुई थी। दुर्भाग्य से आज अधिकांश जल निकायों को आवासों में बदला गया है, लेकिन इमारतों के भीतर गणेश मंदिर रह गए। अब केवल कपित्था और जम्बू फल अर्पित करने वाला श्लोक ही गणेश पूजा के साथ जुड़े हुए जल-संबंध का अंतिम अनुस्मारक है।
इन दो फलों की विशिष्टता यह है कि वे उन जगहों पर उगते हैं जहां भूमिगत पानी है। उन्हें “जलनाड़ी” कहा जाता है – जल-शिराएँ। दक्षिण भारत विशेष रूप से भूमिगत मार्ग के नेटवर्क से भरा हुआ है, जो कदाचित दक्खन पठार के निर्माण के समय रिसनेवाले लावा द्वारा निर्मित है। ये मार्ग वर्षाऋतु में बारिश के पानी से भर जाते हैं। जिन स्थानों पर वर्ष के अधिकांश समय पानी बहता है, उनके पास कुछ किस्म के पेड़ उगते पाए जाते हैं। हमारे ऋषियों द्वारा पहचाने गए लगभग 50 वृक्षों को वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक बृहद संहिता (अध्याय 54) में दर्ज किया था। जहाँ पानी का प्रवाह प्रचुर मात्रा में और सतह के पास होता है, वहाँ बांबी बनती हैं और कपित्था और जम्बू जैसे पेड़ जलनाड़ी और बांबी से विशिष्ट दूरी और दिशा में उगते हैं।

वृक्षों के माध्यम से जलनाड़ी की पहचान अकेले दक्षिण भारत के लिए अद्वितीय नहीं है क्योंकि वराहमिहिर के अनुसार इन वृक्षों का मूल विचार ऋषि सारस्वत ने ही दिया था। महाभारत (शल्य पर्व – 49) में दिए गए एक कथन से यह ज्ञात होता है कि यह ऋषि सरस्वती नदी के पास पैदा हुए थे और रहते थे। एक बार जब लगातार बारह वर्षों तक सूखा पड़ा तो सभी ऋषियों ने सरस्वती नदी का क्षेत्र छोड़ दिया। लेकिन सारस्वत वहीं रहे और सूखे के दौरान जीवित रहे और अपनी वैदिक प्रथाओं को बनाए रखा।
इस कथन से पता चलता है कि सरस्वती एक वर्षा-सिंचित नदी थी और हिमावरित हिमालयी पर्वत द्वारा पोषित नहीं थी। 12 वर्षों के सूखे ने नदी के तल को सूखा बना दिया था, लेकिन ऋषि सारस्वत ने कुछ पेड़ों की उपस्थिति के माध्यम से नदी के भूमिगत चैनलों से पानी प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने जो कुछ भी खोजा वह पीढ़ियों तक हस्तांतरित किया गया और अंत में 98 श्लोकों में बृहद संहिता में दर्ज किया गया।
सारस्वत के अनुसार, अगर प्राकृतिक रूप से उगा हुआ जम्बू पेड़ है, तो उसके उत्तर में 4-1/2 फीट की दूरी पर पानी होगा, और पानी 12 फीट की गहराई पर बह रहा होगा। जम्बू पेड़ के पूर्व में अगर वल्मीक पाई जाती है, तो पानी का स्रोत 12 किमी की गहराई पर चींटी-पहाड़ी के दक्षिण में है। कपित्था वृक्ष के मामले में, व्यक्ति को उसके दक्षिण की ओर 10-1/2 फीट पर सांप के बिल की तलाश करनी चाहिए। यदि बिल है, तो इसका मतलब है कि पानी बिल की उत्तरी दिशा में उपलब्ध है।
इस तरह, कुछ खास पेड़ों के जरिए भूमिगत जल स्रोतों की पहचान की जाती थी। हमारे पूर्वजों ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि इन चिह्नकों (पेड़ों) को द्वारा सुरक्षित करने का सबसे उचित तरीका यह है कि उन्हें दिव्य महत्व दिए जाए। कपित्था और जम्बू को भगवान गणेश का प्रसाद बनाया गया। उन्हें पीपल, बरगद और नीम के पेड़ों के नीचे एक घर दिया गया था क्योंकि वे जल स्रोतों के सर्वोत्तम चिह्नक हैं। इन पेड़ों के पास भरपूर पानी पाया जा सकता है। हम उन्हें मदुरई के प्रसिद्ध मारियम्मन तेप्पाकुलम जैसे पुराने मंदिरों के टैंक के पास देख सकते है। यद्यपि 17वीं शताब्दी में निर्मित, यह कहा जाता है कि 7 फीट ऊंचे मुक्कुरुनि विनायक, जो अब मीनाक्षी मंदिर के बितर स्थित है, इस टैंक को खोदते समय मिले थे। यह सिद्ध करता है कि गणेश की इस मूर्ति को उस क्षेत्र में बहुत पहले स्थापित किया गया था क्योंकि यह क्षेत्र पानी की नस को थामे हुए था। गणेश के ज्यादातर पुराने मंदिरों में पानी से जुड़ी किंवदंतियां हैं।

इस पृष्ठभूमि में, अर्जुन की ओर से बाणों की शय्या पर भीष्म को एक तीर ज़मीन पर मारकर जल चढ़ाने का प्रसंग, जलनाड़ी के ज्ञान का ही हिस्सा लगता है। महाभारत बताता है कि अपने रथ पर खड़े होकर अर्जुन द्वारा चलाया गया तीर जमीन पर उस स्थान पर जा गिरा जो भीष्म पितामह जहां लेटे थे उसकी दक्षिण की ओर था और वहीँ से पानी की एक धार निकली। संभवत: उन्होंने एक चिह्नक पेड़ से पानी के स्रोत का पता लगाया था, जिसने इस प्रकरण के बाद अर्जुन (टर्मिनलिया अर्जुन) नाम प्राप्त किया! सारस्वत का कहना है कि अर्जुन वृक्ष के उत्तर में पाई जाने वाली वल्मीक 21 फीट की गहराई पर चींटी-पहाड़ी के पश्चिम में पानी का संकेतक है। संभवत: बाण चलाने से पहले भीष्म पितामह के अपने परिक्रमा के दौरान, अर्जुन ने पेड़ और वल्मीक के लिए आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया था।
हम इन पेड़ों के पीछे के रहस्य को कब समझेंगे? जब हम कब समझेंगे कि वृक्षों के नीचे और बांबी के पास गणेश और सर्प जैसे देवताओं को स्थापित करने के पीछे श्रेष्ठ ज्ञान है?
जलनाड़ी की पहचान के लिए पेड़ों और वल्मीक का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। वल्मीक, जहां सांप रहते हैं, में दूध छिड़कने की प्रथा का संबंध शायद किसी पारिस्थितिक कारण से जुड़ा हुआ है। गर्मियों में जलनाड़ी सूख जाती थी, जिससे सांपों के भूमिगत आवास काफी गर्म हो जाते थे और बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देते थे। जब लोग नियमित रूप से बिलों में दूध चढ़ाकर साँप की पूजा करते हैं, तो साँपों के घर गर्मीयों में भी ठंडा रहेंगे। इससे सांप अपने आवास में रहते हैं और बाहर निकलकर लोगों के लिए खतरा पैदा नहीं करते।
इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने लोगों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए पूजा के तरीके विकसित किए थे। आज सारस्वत द्वारा उल्लिखित कोई भी वृक्ष बहुतायत में नहीं पाए जाते हैं और इन वृक्षों के विनाश के कारण अब कोई जलमार्ग पहचाना नहीं जा सकता है। कम से कम अब हमें आस-पास देखना चाहिए और प्रकृति का पुनर्निर्माण वैसे करना चाहिए जैसे उसका अस्तित्व पहले था।
ध्यान दें:
1. यहां व्यक्त विचार लेखक के हैं और पी गुरुस के विचारों का जरूरी प्रतिनिधित्व या प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
- गणेश पूजा में छिपे जलविज्ञान का रहस्य - February 26, 2019